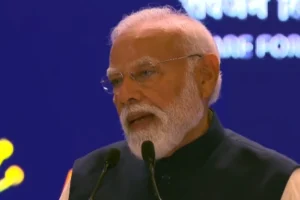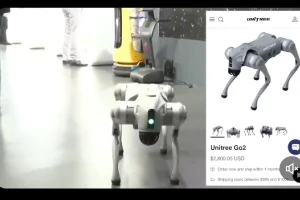भारत द्वारा शेख हसीना प्रत्यर्पण अनुरोध अस्वीकार करने की कानूनी संभावनाएं गहरी
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नया आग्रह और उसके निहितार्थ
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्ज़मान कमाल को भारत से प्रत्यर्पित करने का औपचारिक आग्रह दोबारा करने की घोषणा की है। ढाका से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, दोनों को जुलाई 2024 के छात्रों के आंदोलन के दौरान विरोध कर रहे लोगों की कथित हत्या के प्रकरण में मृत्यु-दंड दिया गया है। इस संदर्भ में अंतरिम प्रशासन के विधिक सलाहकार आसिफ नज़रुल ने स्पष्ट किया कि भारत को भेजे गए पिछले संवाद के अतिरिक्त एक और विस्तृत पत्र शीघ्र भेजा जाएगा।
इस आग्रह के साथ अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मानवाधिकार, न्यायिक निष्पक्षता और दोपक्षीय प्रोटोकॉल की जटिलताएं एक बार फिर उभर आई हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की पृष्ठभूमि को देखते हुए यह मुद्दा स्वाभाविक रूप से संवेदनशील है। किंतु किसी भी राष्ट्र के लिए प्रत्यर्पण का प्रश्न मात्र राजनीतिक नहीं, बल्कि विधिक दायरे से संचालित होता है।
भारतीय कानून और द्विपक्षीय संधि के अंतर्गत अस्वीकार करने का वैधानिक ढांचा
अहमदाबाद स्थित कानूनी विशेषज्ञ आदित्य भट्ट के अनुसार भारत के पास बांग्लादेश के इस अनुरोध को ठुकराने के स्पष्ट और सुदृढ़ कानूनी आधार मौजूद हैं। 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 31 तथा भारत–बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि (2013, संशोधित 2016) के अनुच्छेद 1, 6 और 8, इन आधारों को विस्तृत रूप में दर्शाते हैं।
अनुच्छेद 1 दोनों देशों में कम से कम एक वर्ष की कारावास-योग्य संज्ञेय अपराधों पर प्रत्यर्पण की सामान्य बाध्यता का संकेत देता है, किन्तु यह बाध्यता पूर्णत: अनिवार्य नहीं है। इसे संधि के अन्य अनुच्छेदों में निहित अपवादों के आलोक में देखा जाना आवश्यक है। यही अपवाद भारत को न्याय के हितों और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के लिहाज से विवेकाधिकार प्रदान करते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि अनुच्छेद 6 और 8 इस विवेकाधिकार का वास्तविक आधार हैं। इनमें स्पष्ट है कि यदि प्रेषक देश के अनुरोध में न्यायिक भेदभाव, राजनीतिक प्रतिशोध, यातना या अवमानवीय दंड का जोखिम मौजूद हो, तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है।
शेख हसीना का प्रतिवेदन और आईसीटी पर उठे सवाल
पूर्व प्रधानमंत्री हसीना ने लिखित बयान जारी कर आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे राजनीतिक दमन की मिसाल बताया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 में हुए छात्र-आंदोलन के दौरान उन्होंने सुरक्षा बलों को गोली चलाने का कोई आदेश नहीं दिया। साथ ही, उन्होंने बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) की कार्यप्रणाली को पक्षपातपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया।
आईसीटी की स्थापना मूलतः 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़े युद्ध अपराधों की सुनवाई हेतु की गई थी। समय के साथ 1973 के अंतरराष्ट्रीय अपराध अधिनियम में संशोधन होते रहे, जिसके अनुसार दोष सिद्ध होने पर मृत्युदंड को अधिकतम दंड के रूप में बरकरार रखा गया है। किंतु हालिया मामलों में जिस गति और प्रक्रिया के साथ सुनवाई हुई, उससे न्यायिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।
पूर्व गृहमंत्री कमाल ने भी इस न्यायाधिकरण को असंवैधानिक और अमान्य बताया है। विशेषज्ञों के अनुसार, अनुपस्थित अभियुक्त पर सुनवाई करना, स्वतंत्र विधिक प्रतिनिधित्व का अभाव, तथा शासन परिवर्तन के तुरंत बाद तेज-गति से निर्णय सुनाना – ये सभी तत्व एक निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत के विपरीत हैं।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विवाद और भारत का संवैधानिक दायित्व
कानूनी विशेषज्ञ आदित्य भट्ट का कहना है कि अनुच्छेद 8 के अंतर्गत यदि किसी आरोपी को ऐसे देश में भेजने पर यातना, अमानवीय व्यवहार या अंतरराष्ट्रीय मानकों से कमतर न्याय मिलने का जोखिम हो, तो अनुरोध को अस्वीकार करना संधि के अनुकूल ही है।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायशास्त्र में Soering v. UK जैसे निर्णय प्रमुख मिसाल हैं, जिसमें यह व्यवस्था दी गई कि यदि किसी आरोपी को प्रत्यर्पित करने से उसे न्यायिक अधिकारों के स्पष्ट हनन का जोखिम हो, तो प्रत्यर्पण रोका जा सकता है। मानवाधिकारों की यह न्यायिक परंपरा अब व्यापक रूप से स्वीकृत है।
भारत के संदर्भ में यह दायरा और भी विस्तृत हो जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 देश के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को – चाहे वह भारतीय हो या विदेशी – न्यायोचित प्रक्रिया का अधिकार प्रदान करता है। भारत के न्यायालयों ने बार-बार यह कहा है कि प्रत्यर्पण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि प्रतिपक्षी देश में अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई मिलेगी। बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और मृत्युदंड के अनुपात संबंधी चिंताएं इस संबंध में गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।
ढाका में तनावपूर्ण स्थिति और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य
ढाका में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी को भारी सुरक्षा घेरे में रखा है। जनता में असंतोष और विरोध प्रदर्शनों की आशंका लगातार बढ़ रही है। अगस्त 2024 में लंबे समय तक चले छात्र आंदोलनों के बाद हसीना को पद छोड़ना पड़ा था। आर्थिक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और सत्तावादी प्रवृत्तियों के आरोपों ने आंदोलन को व्यापक समर्थन दिया।
इन आंदोलनों के दौरान हुए हिंसक टकरावों में सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई बताई जाती है, जिसने बांग्लादेश की राजनीति को गहरे संकट में डाल दिया। वर्तमान अंतरिम सरकार न्याय और जवाबदेही पर जोर दे रही है, किन्तु इसके आलोचक इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हैं।
भारत–बांग्लादेश संबंधों की परीक्षा और आगामी संभावनाएं
भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चली आ रही साझेदारी, व्यापार, सुरक्षा सहयोग और सीमा प्रबंधन के मामलों में गहरा तालमेल रहा है। ऐसे में शेख हसीना का मामला द्विपक्षीय संबंधों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि, भारतीय नीति परंपरागत रूप से विधिक प्रक्रियाओं से निर्देशित रही है, और किसी भी राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर न्यायिक मानदंडों को प्राथमिकता देती है।
आगामी समय में प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय भारत की न्यायिक और राजनीतिक व्यवस्था दोनों के सामने एक संवेदनशील परीक्षण होगा। जहाँ एक ओर भारत को मानवाधिकार सिद्धांतों और संवैधानिक दायित्वों के अनुरूप कार्य करना है, वहीं दूसरी ओर दोपक्षीय संबंधों का संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण आयाम है।
ये न्यूज IANS एजेंसी के इनपुट के साथ प्रकाशित हो गई है।