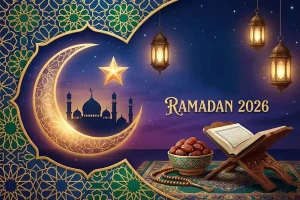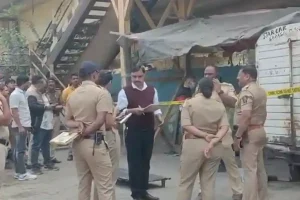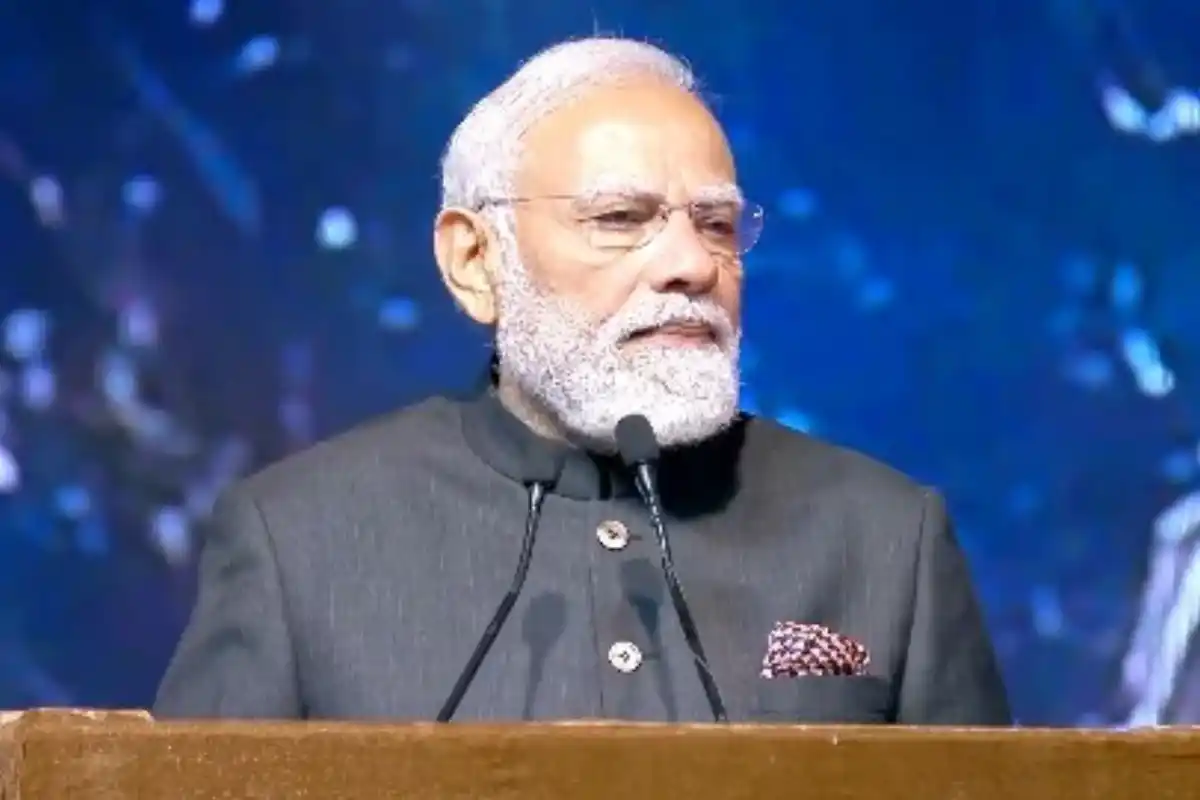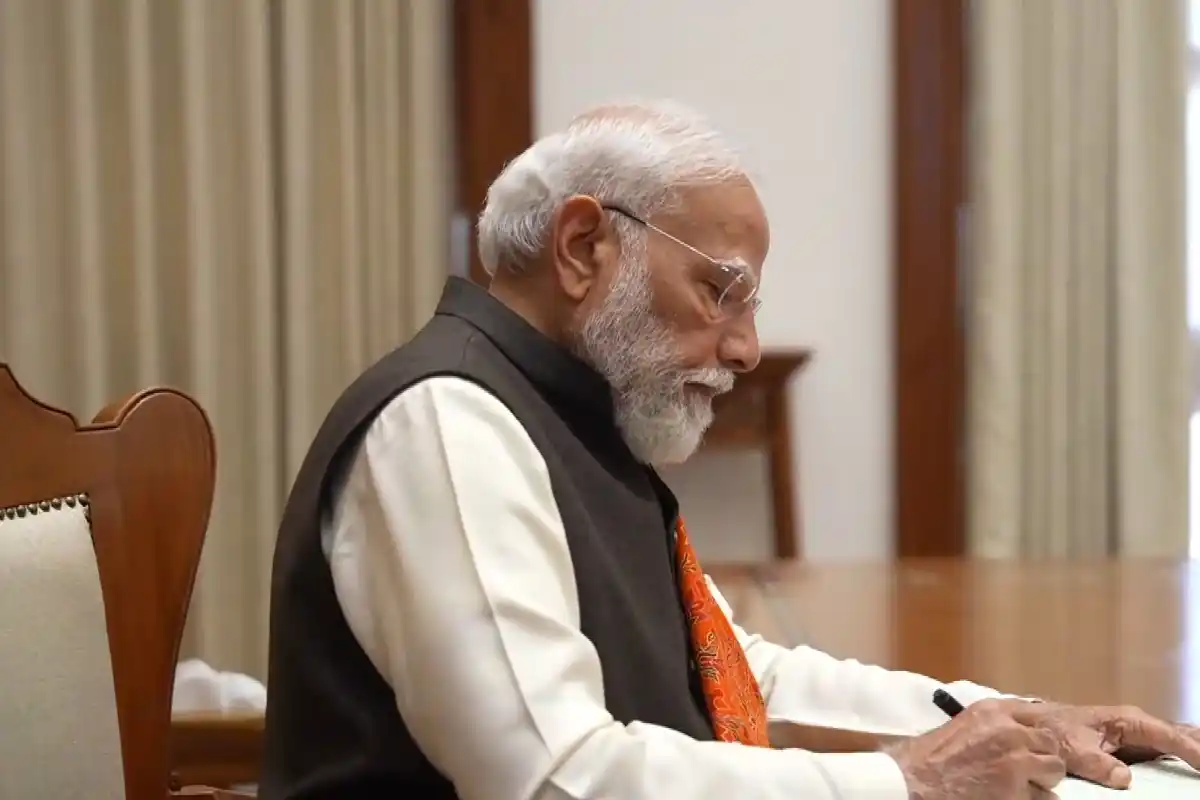दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का विकराल संकट, हर साल बिगड़ रही है हवा की गुणवत्ता
सर्दियों के आते ही दिल्ली और एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में वायु प्रदूषण की समस्या एक बार फिर चरम पर पहुंचने लगती है। पिछले कई वर्षों से यह समस्या केवल मौसमी चिंता नहीं रही, बल्कि अब यह एक स्थायी पर्यावरणीय संकट बन चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए केवल अल्पकालिक उपाय नहीं, बल्कि दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है।
सर्दियों के साथ लौटती ‘ज़हरीली हवा’
नोएडा में आयोजित एक पर्यावरणीय विमर्श में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पूर्व अपर निदेशक डॉ. एस. के. त्यागी ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति हर साल और खराब हो रही है।
उन्होंने कहा, “हर वर्ष सरकारें और संस्थान शॉर्ट टर्म प्लान पर काम कर इतिश्री कर लेते हैं, जबकि हमें लॉन्ग टर्म विज़न अपनाने की ज़रूरत है।”
डॉ. त्यागी ने यह भी कहा कि वायु प्रदूषण के मापदंड अब पुराने हो चुके हैं। साल 2009 में एक्यूआई (AQI) के मानक बनाए गए थे और 2015 में वायु प्रदूषण के मानक तय हुए थे, जबकि पर्यावरण और प्रदूषण की प्रकृति अब पूरी तरह बदल चुकी है।
क्यों जरूरी है मानकों में बदलाव
वाष्पशील कार्बनिक रसायन (VOC) को शामिल करने की जरूरत
डॉ. त्यागी ने बताया कि वायु प्रदूषण में वाष्पशील कार्बनिक रसायन (VOC) को भी शामिल किया जाना चाहिए। ये रसायन कमरे के तापमान पर गैस में बदल जाते हैं और हवा में ग्राउंड लेवल पर पाए जाते हैं।
VOC से ओजोन परत को नुकसान होता है और यह सेकेंड्री ऑर्गेनिक एयरोसोल (SOA) का निर्माण करते हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, PM 2.5 में VOC का योगदान करीब 30 प्रतिशत तक है।
कोविड काल में भी नहीं घटी VOC की मात्रा
कोविड महामारी के दौरान जब सड़कें खाली थीं और औद्योगिक गतिविधियां रुकी हुई थीं, तब भी VOC के स्तर में उल्लेखनीय कमी नहीं आई थी। इसका मतलब है कि इन रसायनों का प्रभाव हवा की गुणवत्ता पर लगातार बना रहता है।
अमेरिका जैसे देशों में VOC मॉनिटरिंग के लिए 90 से अधिक केंद्र हैं, जबकि भारत में अब तक इसकी कोई ठोस व्यवस्था नहीं बन पाई है।
प्रदूषण के प्रमुख कारण और उनका प्रभाव
1. वाहनों से निकलता धुआं
विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली-एनसीआर के प्रदूषण में वाहनों का योगदान 30 से 40 प्रतिशत तक है। डीज़ल वाहनों, पुराने ट्रकों और दोपहिया वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा को सबसे अधिक प्रभावित करता है।
2. औद्योगिक उत्सर्जन
कारखानों और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण में 20 प्रतिशत तक का योगदान देता है।
3. पराली और कचरा जलाना
पराली जलाने से उत्पन्न धुआं प्रदूषण में 3 से 5 प्रतिशत योगदान देता है, जबकि सर्दियों में कूड़ा जलाने से प्रदूषण का स्तर 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ जाता है।
4. निर्माण कार्य
सर्दियों में निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल हवा की गुणवत्ता को तेजी से बिगाड़ देती है। इसलिए डॉ. त्यागी ने सुझाव दिया कि ठंड के मौसम में बड़े निर्माण कार्यों को सीमित किया जाए।
समाधान की दिशा में उठाए जा सकने वाले कदम
सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
विशेषज्ञों ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत किया जाए और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
यदि नागरिक निजी वाहनों की बजाय बस, मेट्रो या साइकिल का प्रयोग करें, तो प्रदूषण में बड़ी कमी आ सकती है।
औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण
औद्योगिक इकाइयों के लिए उत्सर्जन के सख्त मानक तय किए जाने चाहिए और पुराने प्रदूषणकारी संयंत्रों को चरणबद्ध रूप से बंद करना चाहिए।
व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव
-
बिजली की खपत घटाएं और सौर ऊर्जा (Solar Energy) का उपयोग करें।
-
क्लीन कुकिंग फ्यूल (LPG या बायोगैस) का प्रयोग बढ़ाएं।
-
घर के निर्माण में प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन को प्राथमिकता दें।
-
किचन वेस्ट और प्लास्टिक जलाने से बचें।
VOC के दुष्प्रभाव: क्यों हैं ये खतरनाक
कुछ VOC रसायनों के संपर्क में आने से सिरदर्द, आंखों में जलन, और गुर्दे जैसे आंतरिक अंगों को नुकसान हो सकता है।
अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, बच्चे और बुजुर्ग इनसे सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि घर के अंदर VOC की मात्रा अक्सर बाहर की तुलना में अधिक होती है, जिससे “इनडोर एयर क्वालिटी” भी गंभीर समस्या बन रही है।
निष्कर्ष: दीर्घकालिक नीति की है सख्त जरूरत
डॉ. त्यागी और अन्य पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर की हवा को स्वच्छ बनाने के लिए सिर्फ सर्दियों में अल्पकालिक योजनाएँ नहीं, बल्कि सालभर चलने वाली समग्र नीति की आवश्यकता है।
वाहनों, उद्योगों और व्यक्तिगत आदतों में बदलाव के बिना इस “साइलेंट डिजास्टर” से छुटकारा पाना असंभव है।